जयपुर का शहरी भविष्य: सैटेलाइट टाउन की अवधारणा का जनसांख्यिकीय एवं योजनागत विश्लेषण
जयपुर का शहरी भविष्य: सैटेलाइट टाउन की अवधारणा का जनसांख्यिकीय एवं योजनागत विश्लेषण
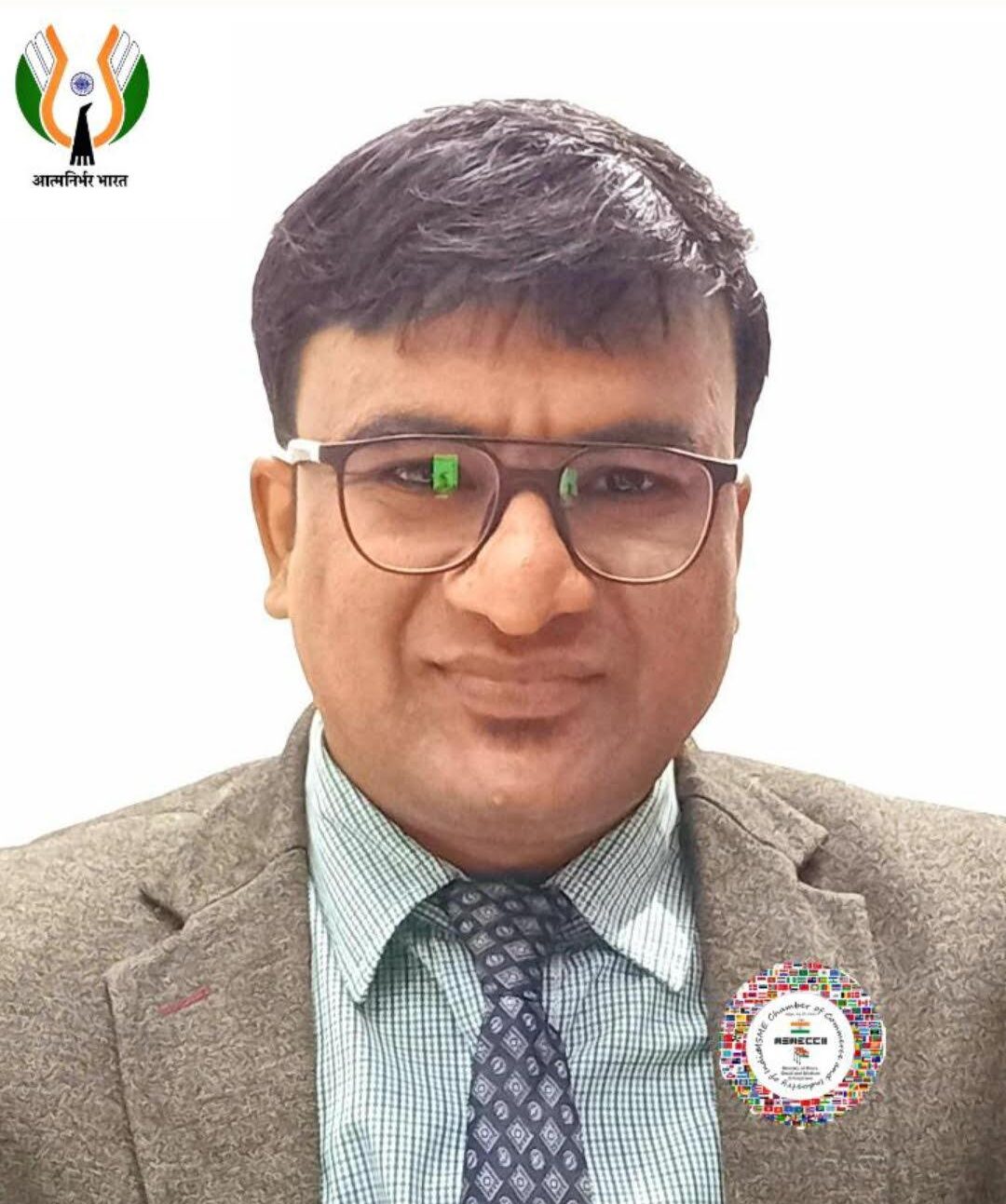
राजस्थान सरकार द्वारा जयपुर के परिधीय कस्बों को सैटेलाइट टाउन के रूप में विकसित करने हेतु फिजिबिलिटी स्टडी आरंभ करने की घोषणा, शहरी नियोजन और जनसंख्या प्रबंधन के दृष्टिकोण से एक अत्यंत महत्वपूर्ण एवं सामयिक हस्तक्षेप है। एक जनसंख्या विज्ञानी और शहरी विकास के स्कॉलर के रूप में, मैं इस कदम को जयपुर पर बढ़ते ‘जनसांख्यिकीय दबाव’ (Demographic Pressure) और ‘नगरीय प्राथमिकीकरण’ (Urban Primacy) की गंभीर होती समस्या के एक तार्किक समाधान के प्रयास के रूप में देखता हूँ। हालाँकि, गुजरात के गिफ्ट सिटी या हैदराबाद के हाईटेक सिटी जैसे सफल मॉडलों का अनुकरण करने की आकांक्षा सराहनीय है, परंतु हमें यह समझना होगा कि शहरी विकास कोई ‘एक आकार सभी के लिए उपयुक्त’ (one-size-fits-all) समाधान नहीं है। इस महत्वाकांक्षी परियोजना की सफलता इसकी घोषणा में नहीं, बल्कि इसके पीछे की वैज्ञानिक सोच, समग्र योजना और क्रियान्वयन की सूक्ष्मता में निहित होगी। यह आलेख इसी परियोजना के विभिन्न आयामों का एक तार्किक और विश्लेषणात्मक विमर्श प्रस्तुत करने का एक प्रयास है, ताकि यह पहल केवल एक और अधूरी शहरी परियोजना बनकर न रह जाए।
किसी भी शहर के विकास को उसकी ‘वाहक क्षमता’ (Carrying Capacity) के संदर्भ में समझा जाना चाहिए। जयपुर, अपनी ऐतिहासिक और प्रशासनिक महत्ता के कारण, दशकों से प्रवासन का एक प्रमुख केंद्र रहा है। ग्रामीण क्षेत्रों से बेहतर शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार की तलाश में होने वाला यह पलायन (Migration) ‘पुल एवं पुश फैक्टर’ की एक क्लासिक गतिकी को दर्शाता है। परिणाम यह हुआ है कि जयपुर की भौतिक और सामाजिक अवसंरचना अपनी वहन क्षमता की सीमा को पार कर चुकी है। आज हम जो ट्रैफिक जाम, जल संकट, आवास की कमी और पर्यावरणीय क्षरण देख रहे हैं, वे केवल कुप्रबंधन के लक्षण नहीं, बल्कि एक ऐसे शहर के संकेत हैं जिसकी जनसंख्या वृद्धि उसकी संस्थागत क्षमता से कहीं आगे निकल चुकी है। सैटेलाइट टाउन की अवधारणा इसी दबाव को विकेंद्रित करने का एक सिद्धान्ततः प्रभावी उपकरण है। लेकिन यहाँ एक मूलभूत प्रश्न उठता है: क्या ये प्रस्तावित टाउन वास्तव में ‘सैटेलाइट’ या ‘उपग्रह’ नगर होंगे अथवा केवल ‘शयनागार उपनगर’ (Dormitory Suburbs)? एक सफल सैटेलाइट टाउन आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर होता है; वह रोजगार सृजित करता है, न कि केवल अपने निवासियों को मुख्य शहर में काम करने के लिए भेजता है। यदि इन नए शहरों को अपनी स्वयं की आर्थिक गतिशीलता प्रदान नहीं की गई, तो ये जयपुर की समस्याओं को कम करने के बजाय, केवल उन्हें भौगोलिक रूप से और अधिक फैला देंगे, जिससे परिवहन नेटवर्क पर दबाव और बढ़ जाएगा।
इस योजना के सफल क्रियान्वयन के लिए हमें इसे कुछ अंतर्संबंधित स्तंभों पर आधारित एक एकीकृत प्रणाली के रूप में देखना होगा। इसका प्रथम और सर्वाधिक महत्वपूर्ण स्तंभ ‘आर्थिक आत्मनिर्भरता’ है। प्रत्येक प्रस्तावित टाउन के लिए एक विशिष्ट आर्थिक क्लस्टर मॉडल विकसित करना होगा। उदाहरणार्थ, दिल्ली-जयपुर आर्थिक गलियारे पर स्थित कोटपूतली को ‘लॉजिस्टिक्स एवं वेयरहाउसिंग हब’ के रूप में विकसित किया जा सकता है। बगरू और चौमूँ को उनके पारंपरिक कौशल (टेक्सटाइल, कृषि) के आधार पर ‘आधुनिक एग्रो-प्रोसेसिंग एवं हैंडीक्राफ्ट क्लस्टर’ का रूप दिया जा सकता है। इसके लिए सरकार को लक्षित प्रोत्साहन (Targeted Incentives), सिंगल-विंडो क्लीयरेंस और प्लग-एंड-प्ले इंफ्रास्ट्रक्चर प्रदान करना होगा ताकि निजी क्षेत्र का निवेश आकर्षित हो। दूसरा स्तंभ ‘मल्टी-मॉडल इंटीग्रेटेड ट्रांजिट सिस्टम’ है। केवल मेट्रो का प्रस्ताव पर्याप्त नहीं है। हमें एक ऐसी एकीकृत परिवहन प्रणाली चाहिए जिसमें रैपिड रेल, बीआरटीएस और एक्सप्रेस-वे का एक सहज नेटवर्क हो, जो न केवल भौतिक दूरी को कम करे, बल्कि यात्रा में लगने वाले समय और लागत को भी न्यूनतम करे, क्योंकि यही कारक किसी शहर की आर्थिक उत्पादकता और जीवन की गुणवत्ता को सीधे प्रभावित करते हैं। तीसरा और समान रूप से महत्वपूर्ण स्तंभ ‘सामाजिक अवसंरचना’ है, जिसे हमें ‘मानव विकास सूचकांक’ (Human Development Index) के पैमाने पर देखना चाहिए। इन शहरों में विश्वस्तरीय स्कूल, अस्पताल, कौशल विकास केंद्र और सार्वजनिक स्थल केवल सुविधाएँ नहीं, बल्कि कुशल मानव पूंजी को आकर्षित करने और बनाए रखने के लिए अनिवार्य निवेश हैं। एक शहर की सफलता अंततः उसके निवासियों की गुणवत्ता से मापी जाती है।
योजना के इस अकादमिक विमर्श में हमें दो व्यावहारिक चुनौतियों को नज़रअंदाज़ नहीं करना चाहिए: भूमि अधिग्रहण और शासन प्रणाली (Governance)। भूमि अधिग्रहण की प्रक्रिया को दंडात्मक होने के बजाय सहभागी (Participatory) होना चाहिए। गुजरात के ‘टाउन प्लानिंग स्कीम’ (TPS) मॉडल का अध्ययन यहाँ प्रासंगिक हो सकता है, जहाँ भू-मालिकों को विकास प्रक्रिया में हितधारक बनाया जाता है। यह न केवल विवादों को कम करता है बल्कि विकास के लाभों का न्यायसंगत वितरण भी सुनिश्चित करता है। जहाँ तक शासन का प्रश्न है, इन नए शहरों के लिए एक पारंपरिक नगर निगम के बजाय एक ‘अधिकार प्राप्त विकास प्राधिकरण’ (Empowered Development Authority) अधिक प्रभावी हो सकता है, जो वित्तीय और प्रशासनिक रूप से स्वायत्त हो। साथ ही, राजस्थान जैसे जल-संवेदनशील राज्य में ‘टिकाऊ शहरीकरण’ (Sustainable Urbanism) के सिद्धांतों को योजना के केंद्र में रखना होगा। वर्षा जल संचयन, अपशिष्ट जल का शत-प्रतिशत पुनर्चक्रण, और हरित भवन संहिताओं को अनिवार्य करना एक विकल्प नहीं, बल्कि एक आवश्यकता है।
अंत में, यह कहना उचित होगा कि जयपुर के लिए सैटेलाइट टाउन की परिकल्पना एक साहसिक और आवश्यक कदम है। यह जयपुर के अनियंत्रित विस्तार पर विराम लगाने और एक अधिक संतुलित क्षेत्रीय विकास का मार्ग प्रशस्त करने का अवसर प्रदान करता है। हालाँकि, इसकी सफलता इस बात पर निर्भर करेगी कि हम इस विचार को कितनी गहराई से समझते हैं। सरकार द्वारा शुरू की गई फिजिबिलिटी स्टडी केवल एक तकनीकी-आर्थिक रिपोर्ट बनकर नहीं रहनी चाहिए, बल्कि इसे एक व्यापक ‘सामाजिक-आर्थिक और पर्यावरणीय प्रभाव आकलन’ का रूप दिया जाना चाहिए। यह परियोजना केवल कंक्रीट और स्टील की नहीं, बल्कि समुदायों के निर्माण, अवसरों के सृजन और भविष्य की पीढ़ियों के लिए एक बेहतर और अधिक टिकाऊ राजस्थान बनाने की है। यह एक ऐसा क्षण है जहाँ दूरदर्शी योजना, दृढ़ राजनीतिक इच्छाशक्ति और विशेषज्ञतापूर्ण क्रियान्वयन मिलकर शहरी इतिहास की एक नई इबारत लिख सकते हैं।
लेखक : डॉ नयन प्रकाश गांधी अंतराष्ट्रीय जनसंख्या विज्ञान संस्थान ,मुंबई विश्विद्यालय के एलुमनाई रहे है और भारत के प्रख्यात नेशनल यूथ एक्सीलेंस अवॉर्डी ,युवा मैनेजमेंट विश्लेषक डेवलेपमेंट प्रैक्टिशनर है , वर्तमान में शहरीकरण में रिसर्च अध्ययन में सक्रिय है । राज्य एवं राष्ट्रीय स्तर पर समसामयिक पब्लिक पॉलिसी विषयों पर लगातार सक्रिय है ।

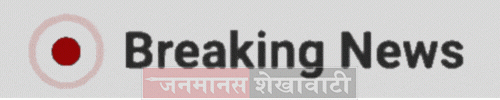

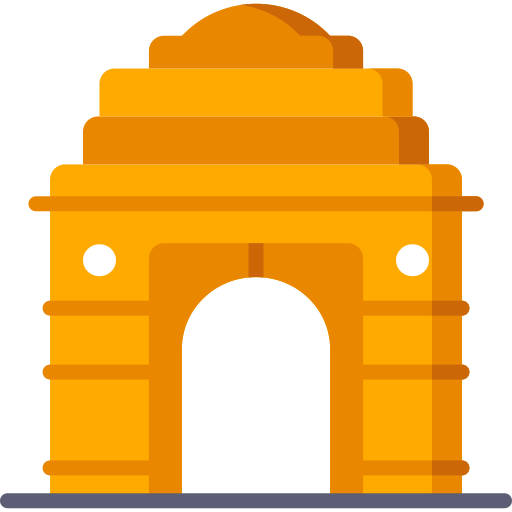 देश
देश विदेश
विदेश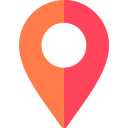 प्रदेश
प्रदेश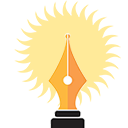 संपादकीय
संपादकीय वीडियो
वीडियो आर्टिकल
आर्टिकल व्यंजन
व्यंजन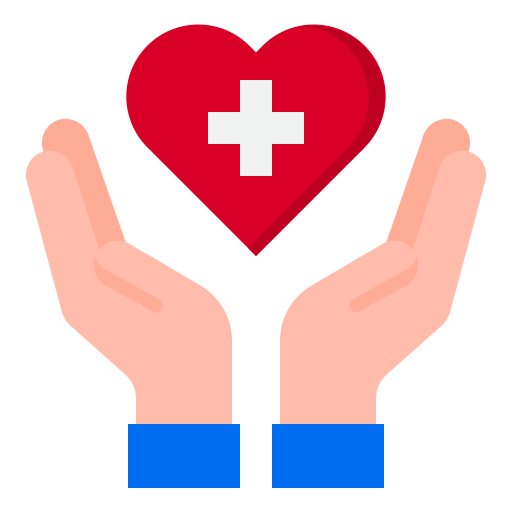 स्वास्थ्य
स्वास्थ्य बॉलीवुड
बॉलीवुड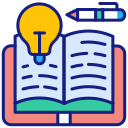 G.K
G.K खेल
खेल बिजनेस
बिजनेस गैजेट्स
गैजेट्स पर्यटन
पर्यटन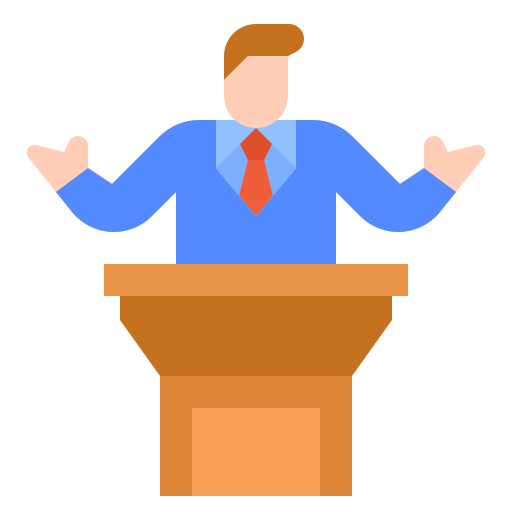 राजनीति
राजनीति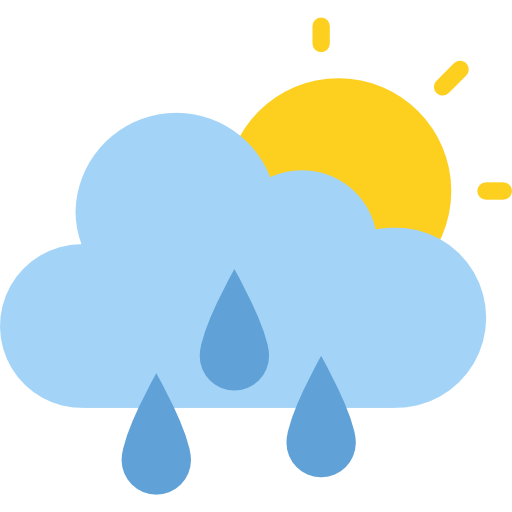 मौसम
मौसम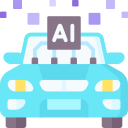 ऑटो-वर्ल्ड
ऑटो-वर्ल्ड करियर/शिक्षा
करियर/शिक्षा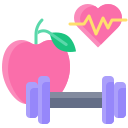 लाइफस्टाइल
लाइफस्टाइल धर्म/ज्योतिष
धर्म/ज्योतिष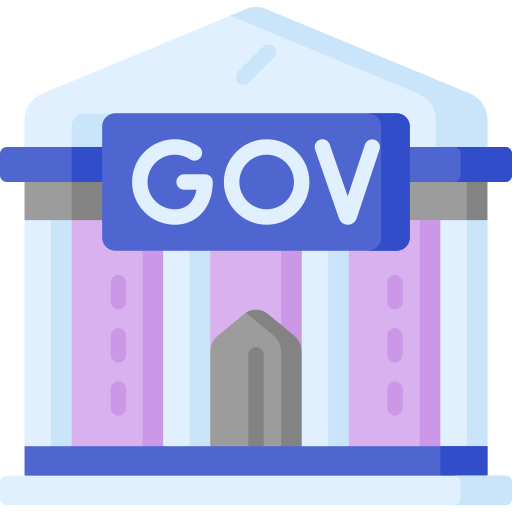 सरकारी योजना
सरकारी योजना फेक न्यूज एक्सपोज़
फेक न्यूज एक्सपोज़ मनोरंजन
मनोरंजन क्राइम
क्राइम चुनाव
चुनाव ट्रेंडिंग
ट्रेंडिंग Covid-19
Covid-19







 Total views : 2019451
Total views : 2019451


