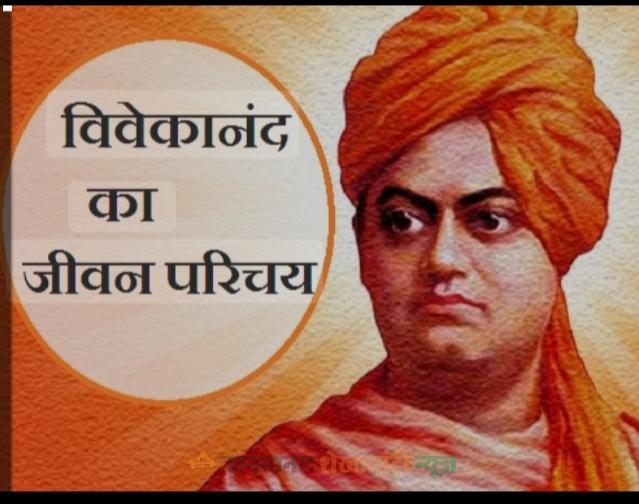
“नरेन्द्र वास्तव में एक जीनियस है। मैंने काफी विस्तृत और बड़े इलाकों में यात्रा की है लेकिन उनकी जैसी प्रतिभा वाला का एक भी बालक कहीं नहीं देखा यहाँ तक की जर्मन विश्वविद्यालयों के दार्शनिक छात्रों में भी नहीं।” अनेक बार इन्हें श्रुतिधर( विलक्षण स्मृति वाला एक व्यक्ति) भी कहा गया है।” विलियम हेस्टी, प्रिंसिपल, जनरल असेम्बली इंस्टिटूशन, कलकत्ता

भारत में विवेकानन्द को एक देशभक्त सन्यासी के रूप में माना जाता है और उनके जन्मदिन को राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में मनाया जाता है।

“अध्यात्म-विद्या और भारतीय दर्शन के बिना विश्व अनाथ हो जायेगा।” स्वामी विवेकानंद
परिचय :
नाम – नरेंद्र नाथ दत्त
उपनाम – विवेकानंद (विवेक का आनंद)
जन्म – 12 जनवरी 1863 (मकर संक्रान्ति संवत् 1920)
जन्म स्थान – मोहन स्कट्रीट कलकत्ता, बंगाल (1877 में परिवार कुछ समय के लिए रायपुर चला गया।)
मृत्यु – 4 जुलाई 1902
शांत स्थान – बेल्लूर मठ हावड़ा, बंगाल
पिता – विश्वनाथ दत्त (कलकत्ता हाई कोर्ट में वकील)
माता – भुवनेश्वरी देवी (गृहणी, शिव की उपासक)
जाति – बंगाली कायस्थ
दादा – दुर्गाचरण दत्ता, संस्कृत एवं फ़ारसी के विद्वान 25 वर्ष की आयु में गृहस्थी त्याग कर वैराग ले लिया।
नाना – नंदलाल बसु
दर्शन – वेदान्त
कार्य – आध्यात्मिक गुरु, लेखक,उपदेशक
विश्व धर्म सम्मेलन शिकागो – अमेरिका स्थित शिकागो में सन् 1893 में आयोजित विश्व धर्म महासभा में भारत की ओर से ब्राह्मण (सनातन) धर्म का प्रतिनिधित्व किया।
गुरु –
नवम्बर 1881 रामकृष्ण परमहंस से प्रथम भेंट
स्वामी रामकृष्ण परमहंस (16 अगस्त 1986 में मृत्यु)
संस्था – रामकृष्ण मिशन की स्थापना
भाषा –
अंग्रेजी
बंगाली
संस्कृत
शिक्षा –
प्रारंभिक शिक्षा – आठ वर्ष की आयु में (1871) ईश्वर चंद्र विद्यासागर के मेट्रोपोलिटन संस्थान, स्कूल से प्रारंभ।
उच्च शिक्षा
1. वर्ष 1879 कलकत्ता के प्रेसीडेंसी कॉलेज प्रवेश परीक्षा 1879 में प्रथम श्रेणी से उत्तीर्ण।
2. स्कॉटिश चर्च कॉलेज (जनरल असेम्बली इंस्टिटूशन, कलकत्ता) से पाश्चात्य तर्क -शास्त्र, दर्शन और इतिहास का अध्ययन किया।
3. वर्ष 1881 में ललित कला परीक्षा उत्तीर्ण और 1884 में कला स्नातक डिग्री पूर्ण की।
4. भारतीय शास्त्रीय संगीत का ज्ञान प्राप्त किया।
मठ स्थापना – 1886 वराहनगर में
अध्यात्म के अलावा रुचि
नरेन्द्र भारतीय दर्शन के साथ – साथ पश्चिमी लेखकों, डेविड ह्यूम, इमैनुएल कांट, जोहान गोटलिब फिच, बारूक स्पिनोज़ा, जोर्ज डब्लू एच हेजेल, आर्थर स्कूपइन्हार , ऑगस्ट कॉम्टे, जॉन स्टुअर्ट मिल और चार्ल्स डार्विन की पुस्तकों का गहराई से पठन किया। वर्ष 1860 में प्रकाशित हरबर्ट स्पेंसर की पुस्तक एजुकेशन का बंगाली भाषा में अनुवाद किया। नरेंद्र, स्पेंसर के विकासवाद के सिद्धांत से अत्यधिक प्रभावित थे।
नरेंद्र से विवेकानंद, लक्ष्य का निर्धारण
“उठो चलो और तब तक मत रुको जब तक लक्ष्य प्राप्त ना कर लो।”
कहानी 01- एक बार स्वामी जी आश्रम में सो रहे थे। उनके पास एक दुखी व्यक्ति ने आ कर निवेदन किया कि “महाराज मैं लगन और मेहनत से कमाता हूँ पर सफल व्यक्ति नहीं बन पाया।” स्वामी विवेकानंद ने उस व्यक्ति से कहा “ठीक है, आप मेरे कुत्ते को थोड़ी देर घुमाकर लाये तब तक मैं आपकी समस्या का हल ढूँढ़ता हूँ। वह व्यक्ति कुत्ते को घुमाने हेतु ले गया, काफी देर बाद लौटने पर स्वामी विवेकानन्द ने उस व्यक्ति से पूछा कि यह कुत्ता इतना हाँफ क्यों रहा है? और आप बिल्कुल भी नहीं थके। आगंतुक ने प्रत्युत्तर में कहा “मैं तो सीधा रस्ते पर चल रहा था,पर यह इधर – उधर भागता रहा, कुछ भी देखा उसकी ओर दौड़ने लगता है। यही कारण है कि यह इतना थका हुआ है। स्वामी जी ने मुस्कुरा कर कहा “बस यही तुम्हारे प्रश्नों का उत्तर है। सफलता की मंजिल सामने है पर तुम उसके बजाय इधर – उधर दौड़ते हो, यही कारण है कि तुम जीवन में कभी सफल नही हो पाए।
नारी का सम्मान
उत्तम पुरुष वही है जो हर परिस्थिति में नारी का सम्मान करे।
कहानी 02- स्वामी जी एक समारोह में भागीदारी हेतु विदेश गए। उनके भाषण से एक विदेशी महिला प्रभावित हो कर उनके पास आकर निवेदन किया कि “मैं आपसे विवाह करना चाहती हूँ ताकि आपके जैसे पुत्र को जन्म दे सकूं।” जवाब में स्वामी जी ने कहा ”मै एक सन्यासी हूँ, विवाह नहीं कर सकता, यदि आप चाहें तो मुझे अपना पुत्र बना लीजिए। इससे मेरा सन्यास भी नही टूटेगा और आपको मेरे जैसा पुत्र भी मिल जाएगा।” महिला ने भावपूर्ण धन्यवाद दिया और चली गई।
गुरुभक्त
कहानी 03 – एक बार एक शिष्य ने गुरु परमहंस की सेवा के प्रति घृणा व्यक्त की। स्वामी जी ने यह कार्य स्वयं करना प्रारंभ कर दिया। गुरु परमहंस जी के रक्त, कफ आदि से भरी थूकदानी उठाते। गुरुदेव का शरीर अत्यन्त रुग्ण हो गया था। गुरुदेव के शरीर-त्याग के दिनों में अपने घर और कुटुम्ब की नाजुक हालत व स्वयं के भोजन की चिन्ता किये बिना वे गुरु की सेवा में सतत लगे रहे।
स्वामी जी गुरु के प्रति इस अनन्य भक्ति और निष्ठा के प्रताप से उनके दिव्यतम आदर्शों को प्राप्त कर सके।
“गुरु के अस्तित्व में स्वयं को विलीन करना ही गुरु भक्ति है।”
उनके महान व्यक्तित्व की नींव में गुरुभक्ति, गुरुसेवा और गुरु के प्रति अनन्य निष्ठा जिसका परिणाम सारे संसार ने देखा।
विवेकानंद के शिक्षा के प्रति विचार एवं वेदांत दर्शन
विवेकानन्द बड़े स्वप्नदृष्टा थे। उन्होंने वेदान्त के सिद्धान्तों पर आधारित समाज की कल्पना की, जिसमें धर्म या जाति के आधार पर मनुष्य-मनुष्य में कोई भेद न हो। अध्यात्मवाद बनाम भौतिकवाद के विवाद में पड़े बिना सबल बौद्धिक आधार पर विवेकानंद ने समता के सिद्धान्त दिया। विवेकानन्द को युवकों से बड़ी आशाएँ थीं। स्वामी जी का जीवन युवकों हेतु आदर्श जीवन है। स्वामी जी मैकाले की अंग्रेजी शिक्षा व्यवस्था के विरोधी थे, क्योंकि इस शिक्षा का उद्देश्य सिर्फ बाबुओं की संख्या बढ़ाना था। वह ऐसी शिक्षा चाहते थे जिससे बालक का सर्वांगीण विकास हो सके। शिक्षा का उद्देश्य व्यक्ति को आत्मनिर्भर बना कर स्वयं के पैरों पर खड़ा करना है। स्वामी विवेकानन्द प्रचलित शिक्षा को निषेधात्मक शिक्षा की संज्ञा देते हुए कहते थे।
“आप उस व्यक्ति को शिक्षित मानते हैं जिसने कुछ परीक्षाएं उत्तीर्ण कर ली हों तथा जो अच्छे भाषण दे सकता हो, पर वास्तविकता यह है कि जो शिक्षा जनसाधारण को जीवन संघर्ष के लिए तैयार नहीं करती, जो चरित्र निर्माण नहीं करती, जो समाज सेवा की भावना विकसित नहीं करती तथा जो शेर जैसा साहस पैदा नहीं कर सकती, ऐसी शिक्षा से क्या लाभ ?”
इसलिए स्वामी जी सैद्धान्तिक शिक्षा के पक्षधर न हो कर व्यावहारिक शिक्षा के समर्थक थे।
“शिक्षा ही व्यक्ति को भविष्य हेतु तैयार करती है, इसलिए शिक्षा में उन तत्वों का होना आवश्यक है, जो भविष्य हेतु महत्वपूर्ण हों।”
उनके विचार –
“तुमको कार्य के सभी क्षेत्रों में व्यावहारिक बनना पड़ेगा। सिद्धान्तों के ढेरों ने सम्पूर्ण देश का विनाश कर दिया है।”
स्वामी जी शिक्षा के माध्यम से व्यक्ति को लौकिक एवं पारलौकिक जीवन हेतु तैयार करना चाहते थे। लौकिक दृष्टि से शिक्षा के सम्बन्ध में उन्होंने कहा है कि
‘हमें ऐसी शिक्षा चाहिए, जिससे चरित्र का गठन हो, मन का बल बढ़े, बुद्धि का विकास हो और व्यक्ति स्वावलम्बी बने।’ पारलौकिक दृष्टि से उन्होंने कहा है कि – शिक्षा मनुष्य की अन्तर्निहित पूर्णता की अभिव्यक्ति है।’
कैसी हो शिक्षा व्यवस्था
स्वामी जी का शिक्षा दर्शन मनुष्य-निर्माण की प्रक्रिया पर केन्द्रित है न कि केवल किताबी ज्ञान पर।
एक पत्र में वे लिखते हैं
“शिक्षा क्या है? क्या वह पुस्तक-विद्या है ? नहीं, क्या वह नाना प्रकार का ज्ञान है ? नहीं, यह भी नहीं। जिस संयम के द्वारा इच्छाशक्ति का प्रवाह और विकास वश में लाया जाता है और वह फलदायक होता है, वह शिक्षा कहलाती है।”
शिक्षा के माध्यम से चरित्र निर्माण हेतु विवेकानंद कहते हैं
“शिक्षा का मतलब यह नहीं है कि तुम्हारे दिमाग़ में ऐसी बहुत-सी बातें इस तरह ठूँस दी जाएं, जो आपस में, लड़ने लगें और तुम्हारा दिमाग़ उन्हें जीवन भर हज़म न कर सके। जिस शिक्षा से हम अपना जीवन-निर्माण कर सकें, मनुष्य बन सकें, चरित्र-गठन कर सकें और विचारों का सामंजस्य कर सकें, वही वास्तव में शिक्षा कहलाने योग्य है। यदि तुम पाँच ही भावों को हज़म कर तदनुसार जीवन और चरित्र गठित कर सके हो तो तुम्हारी शिक्षा उस आदमी की अपेक्षा बहुत अधिक है, जिसने एक पूरी की पूरी लाइब्रेरी ही कण्ठस्थ कर ली है।”
देश की आर्थिक, आध्यात्मिक और लौकिक उन्नति में स्वामी जी शिक्षा की केंद्रीय भूमिका मानते थे।
भारत तथा पश्चिम के बीच के अन्तर को वे इसी दृष्टि से वर्णित करते हुए कहते हैं
“केवल शिक्षा! शिक्षा! शिक्षा! यूरोप के बहुतेरे नगरों में घूमकर और वहाँ के ग़रीबों के भी अमन-चैन और विद्या को देखकर हमारे ग़रीबों की बात याद आती थी और मैं आँसू बहाता था। यह अन्तर क्यों हुआ? उत्तर पाया – शिक्षा!” स्वामी विवेकानंद का विचार था कि उपयुक्त शिक्षा के माध्यम से व्यक्तित्व विकसित होना चाहिए और चरित्र की उन्नति होनी चाहिए।”
सन् 1900 में लॉस एंजिल्स, कैलिफ़ोर्निया में दिए गए एक व्याख्यान में स्वामी जी यही बात सामने रखते हैं –
“हमारी सभी प्रकार की शिक्षाओं का उद्देश्य तो मनुष्य के इसी व्यक्तित्व का निर्माण होना चाहिये। परन्तु इसके विपरीत हम केवल बाहर से पालिश करने का ही प्रयत्न करते हैं। यदि भीतर कुछ सार न हो तो बाहरी रंग चढ़ाने से क्या लाभ? शिक्षा का लक्ष्य अथवा उद्देश्य तो मनुष्य का विकास ही है।”
स्वामी विवेकानन्द के आधारभूत शिक्षा सिद्धान्त
1. शिक्षा ऐसी हो जिससे बालक का शारीरिक, मानसिक एवं आत्मिक विकास हो सके।
2. शिक्षा व्यवस्था ऐसी हो जिससे बालक के चरित्र का निर्माण हो, मन का विकास हो, बुद्धि विकसित हो तथा बालक आत्मनिर्भर बने।
3. बालक एवं बालिकाओं दोनों को समान शिक्षा देनी चाहिए।
4. धार्मिक शिक्षा, पुस्तकों आधारित ना होकर आचरण एवं संस्कार आधारित हो।
5. पाठ्यक्रम में लौकिक एवं पारलौकिक दोनों प्रकार के विषयों को स्थान देना चाहिए।
6. शिक्षा, गुरू आश्रम में भी प्राप्त की जा सकती है।
7. शिक्षक एवं छात्र का सम्बन्ध अधिक से अधिक निकट का होना चाहिए।
8. सर्वसाधारण में शिक्षा का प्रचार – प्रसार किया जान चाहिये।
9. देश की आर्थिक प्रगति हेतु तकनीकी शिक्षा की व्यवस्था की जाए।
10. मानवीय एवं राष्ट्रीय शिक्षा परिवार से ही शुरू करनी चाहिए।
12. शिक्षा ऐसी हो जो सीखने वाले को जीवन संघर्ष में आगे बढ़ने की प्रेरणा मिले।
अध्यात्म से लगाव
विद्यालय शिक्षा के साथ-साथ घर पर प्रतिदिन पूजा-पाठ के माहौल के कारण नरेंद की मानसिकता धार्मिक कार्यों एवं अध्यात्म की ओर हुई। अध्यात्म और धार्मिक वातावरण के कारण बालपन में ही उनके मन में ईश्वर की पहचान की चेष्टा जागी। इस हेतु वेद, उपनिषद, भगवद् गीता, रामायण, महाभारत और पुराणों के अतिरिक्त अनेक ब्राह्मण शास्त्रों का गहन रूचि से अध्ययन किया। नरेन्द्र के माता – पिता की धार्मिक क्रियाशीलता ने उनके व्यक्तित्व में प्रगतिशीलता एवं तर्कसंगतता की भावना का विकास किया। वर्ष 1880 में नरेन्द, केशवचन्द्र सेन की संस्था नव विधान में शामिल हुए। यह संस्था देवेन्द्र नाथ टैगोर और केशव चंद्र सेन द्वारा संचालित साधारण ब्रह्म समाज, ब्रह्म समाज का भाग था। नरेंद्र वर्ष 1881 से 1884 के समय ‘Sence Band Of Hope’ में भी सक्रीय रहे जो धूम्रपान और शराब के नशे से युवाओं को बचाने का कार्य करती थी। शुरुआत में नरेंद्र ब्रह्म समाज के सिद्धांत एक एवं निराकार ईश्वर में विश्वास रखते हुए मूर्ति पूजा का विरोध किया। बाद में नरेंद्र सनातन गुरु रामकृष्ण देव (परमहंस) से प्रभावित हुए। परमहंस ने अद्वैतवादी अवधारणाओं से तराश कर नरेंद्र को तर्कशील, विचारशील, भाषण में पारंगतता के साथ वेदांत और उपनिषदों का आधुनिक ढंग से अध्ययन करने हेतु प्रोत्साहित किया। गुरु रामकृष्ण देव से काफी प्रभावित हो कर उन्होंने सीखा कि सारे जीवों मे स्वयं परमात्मा का ही अस्तित्व हैं। इसलिए मानव जाति अथेअथ जो मनुष्य दूसरे जरूरतमन्दो की सहायता करता है। मानव सेवा से ही परमात्मा की सेवा की जा सकती है। रामकृष्ण की मृत्यु के बाद विवेकानन्द ने पैदल ही भारत – यात्रा पर निकल कर ब्रिटिश भारत की तत्कालीन परिस्थितियों का प्रत्यक्ष अनुभव किया।
विश्व धर्म सम्मेलन 1893
31 मई 1893 को 25 वर्ष की आयु में नरेन्द्र भगवा धारण कर भारत की पैदल यात्रा पर निकले। इसके बाद वे जापान पहुंचे जहां के कई शहरों (कोबे, नागासाकी, योकोहामा, ओसाका, क्योटो और टोक्यो) का दौरा किया। इसके बाद चीन से कनाडा होते हुए वो अमेरिका के शिकागो पहुँचे। सन् 1893 में शिकागो (अमरीका) में विश्व धर्म परिषद् हो रही थी। स्वामी विवेकानन्द उसमें भारत के प्रतिनिधि के रूप में पहुँचे। योरोप एवं अमरीका वासी गुलाम भारतीयों को हीन दृष्टि से देखते थे। वहाँ लोगों ने बहुत प्रयत्न किया कि स्वामी विवेकानन्द को सर्वधर्म परिषद् में बोलने का समय ना मिले। अमेरिकन प्रोफेसर के प्रयास से उन्हें के केवल दो मिनट का समय मिला। नरेंद्र के विचार सुनकर सभी विद्वान चकित रह गए। अमरीका में जगह – जगह उनका स्वागत हुआ। वहाँ उनके भक्तों का एक बड़ा समुदाय बन गया। 1896 तक तीन वर्ष लगातार अमरीका में रहे। उनकी वक्तृत्व-शैली तथा ज्ञान को देखते हुए वहाँ के मीडिया ने उन्हें साइक्लॉनिक हिन्दू का नाम दिया। दो मिनट के समय को उन्होंने इस तरह बांधा कि सब चकित।
भाषण का आरम्भ “मेरे अमेरिकी बहनों एवं भाइयों” के साथ करने के लिये जाना जाता है। उनके संबोधन के इस प्रथम वाक्य ने सबका दिल जीत लिया। उस समय विवेकानंद की आयु तीस वर्ष थी।
भाषण का अंश (हिंदी)
मेरे अमरीकी बहनों और भाइयों,
आपने जिस सम्मान सौहार्द और स्नेह के साथ हम लोगों का स्वागत किया हैं उसके प्रति आभार प्रकट करने के निमित्त खड़े होते समय मेरा हृदय अवर्णनीय हर्ष से पूर्ण हो रहा हैं। संसार में संन्यासियों की सबसे प्राचीन परम्परा की ओर से मैं आपको धन्यवाद देता हूँ, धर्मों की माता की ओर से धन्यवाद देता हूँ, और सभी सम्प्रदायों एवं मतों के कोटि कोटि हिन्दुओं की ओर से भी धन्यवाद देता हूँ। मैं इस मंच पर से बोलने वाले उन कतिपय वक्ताओं के प्रति भी धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ जिन्होंने प्राची के प्रतिनिधियों का उल्लेख करते समय आपको यह बतलाया है कि सुदूर देशों के ये लोग सहिष्णुता का भाव विविध देशों में प्रचारित करने के गौरव का दावा कर सकते हैं। मैं एक ऐसे धर्म का अनुयायी होने में गर्व का अनुभव करता हूँ जिसने संसार को सहिष्णुता तथा सार्वभौम स्वीकृत- दोनों की ही शिक्षा दी हैं। हम लोग सब धर्मों के प्रति केवल सहिष्णुता में ही विश्वास नहीं करते वरन समस्त धर्मों को सच्चा मान कर स्वीकार करते हैं। मुझे ऐसे देश का व्यक्ति होने का अभिमान है जिसने इस पृथ्वी के समस्त धर्मों और देशों के उत्पीड़ितों और शरणार्थियों को आश्रय दिया है। मुझे आपको यह बतलाते हुए गर्व होता हैं कि हमने अपने वक्ष में उन यहूदियों के विशुद्धतम अवशिष्ट को स्थान दिया था, जिन्होंने दक्षिण भारत आकर उसी वर्ष शरण ली थी जिस वर्ष उनका पवित्र मन्दिर रोमन जाति के अत्याचार से धूल में मिला दिया गया। ऐसे धर्म का अनुयायी होने में मैं गर्व का अनुभव करता हूँ जिसने महान जरथुष्ट जाति के अवशिष्ट अंश को शरण दी और जिसका पालन वह अब तक कर रहा है।
भाईयो, मैं आप लोगों को एक स्त्रोत की कुछ पंक्तियाँ सुनाता हूँ जिसकी आवृति मैं बचपन से कर रहा हूँ और जिसकी आवृति प्रतिदिन लाखों मनुष्य किया करते हैं
रुचीनांवैचित्र्यादृजुकुटिलनानापथजुषाम्।
नृणामेको गम्यस्त्वमसि पयसामर्णव इव॥
अर्थात जैसे विभिन्न नदियाँ भिन्न भिन्न स्रोतों से निकलकर समुद्र में मिल जाती हैं उसी प्रकार हे प्रभु, भिन्न-भिन्न रुचि के अनुसार विभिन्न टेढ़े-मेढ़े अथवा सीधे रास्ते से जाने वाले लोग अन्त में तुझ में ही आकर मिल जाते हैं।
यह सभा, जो अभी तक आयोजित सर्वश्रेष्ठ पवित्र सम्मेलनों में से एक है स्वतः ही गीता के इस अद्भुत उपदेश का प्रतिपादन एवं जगत के प्रति उसकी घोषणा करती है
ये यथा मां प्रपद्यन्ते तांस्तथैव भजाम्यहम्।
मम वर्त्मानुवर्तन्ते मनुष्याः पार्थ सर्वशः॥
अर्थात जो कोई मेरी ओर आता है-चाहे किसी प्रकार से हो, मैं उसको प्राप्त होता हूँ। लोग भिन्न मार्ग द्वारा प्रयत्न करते हुए अन्त में मेरी ही ओर आते हैं।
साम्प्रदायिकता, हठधर्मिता और उनकी वीभत्स वंशधर धर्मान्धता इस सुन्दर पृथ्वी पर बहुत समय तक राज्य कर चुकी है। वे पृथ्वी को हिंसा से भरती रही हैं व उसको बारम्बार मानवता के रक्त से नहलाती रही हैं, सभ्यताओं को ध्वस्त करती हुई पूरे के पूरे देशों को निराशा के गर्त में डालती रही हैं। यदि ये वीभत्स दानवी शक्तियाँ न होतीं तो मानव समाज आज की अवस्था से कहीं अधिक उन्नत हो गया होता। पर अब उनका समय आ गया हैं और मैं आन्तरिक रूप से आशा करता हूँ कि आज सुबह इस सभा के सम्मान में जो घण्टा ध्वनि हुई है वह समस्त धर्मान्धता का, तलवार या लेखनी के द्वारा होने वाले सभी उत्पीड़नों का तथा एक ही लक्ष्य की ओर अग्रसर होने वाले मानवों की पारस्पारिक कटुता का मृत्यु निनाद सिद्ध हो।
विदेश यात्राएं –
विवेकानन्द ने जापान ,चीन, कनाडा, संयुक्त राज्य अमेरिका, इंग्लैंड और यूरोप के कई देशों में ब्राह्मण दर्शन के सिद्धान्तों का प्रसार किया और कई सार्वजनिक और निजी व्याख्यानों का आयोजन किया।
अमरीका में उन्होंने रामकृष्ण मिशन की अनेक शाखाएँ स्थापित कीं। अनेक अमरीकी विद्वानों ने उनका शिष्यत्व ग्रहण किया। स्वामी जी खुद को ‘गरीबों का सेवक’ कहते थे।
राष्ट्रीय संत और उनका योगदान –
केवल उन्चालीस वर्ष के छोटे से जीवन में स्वामी विवेकानन्द के कार्य आने वाली सदियों तक पीढ़ियों का मार्गदर्शन करते रहेंगे। विवेकानंद केवल सन्त ही नहीं, अपितु एक महान देशभक्त, वक्ता, विचारक, लेखक और मानवता-प्रेमी थे। अमेरिका से लौटकर उन्होंने देशवासियों का आह्वान करते हुए कहा
“नया भारत निकल पड़े मोची की दुकान से, भड़भूँजे के भाड़ से, कारखाने से, हाट से, बाजार से; निकल पडे झाड़ियों, जंगलों, पहाड़ों, पर्वतों से।”
स्वामी जी ने गांधी जी के स्वतंत्रता आंदोलन हेतु जन-समर्थन हेतु आह्वान किया। स्वामी जी भारत को धर्म एवं दर्शन की पुण्यभूमि मानते थे। स्वामी जी अहिंसा के स्थान पर सशस्त्र क्रान्ति के माध्यम से भारत को स्वतंत्र करवाना चाहते थे। अपरिपक्व जन आंदोलन के कारण जल्द ही उन्हें अनुभूति हो गई कि परिस्थितियाँ उनके इरादों के अनुकूल नहीं हैं। अब स्वामी जी ने ‘एकला चलो‘ की नीति अपनाई। दर्शन और वेदांत दर्शन के प्रचार में एक परिव्राजक के रूप में संपूर्ण भारत और विश्व का भ्रमण किया।
“मुझे बहुत से युवा संन्यासी चाहिये जो भारत के गांवों में फैलकर देशवासियों की सेवा में खप जायें।” विवेकानंद
अफसोस उनका यह सपना पूरा न हो सका।
विवेकानन्द ने पुरोहितवाद, आडम्बर, कठमुल्लापन और रूढ़ियों के प्रबल विरोध करते हुए धर्म को मनुष्य की सेवा के केन्द्र में रख कर आध्यात्मिक चिंतन किया।
उनके इस आह्वान से पुरोहित वर्ग ने असहमति व्यक्त की।
“धरती की गोद में यदि ऐसा कोई देश है जिसने मनुष्य की हर तरह की बेहतरी के लिए ईमानदार कोशिशें की हैं, तो वह भारत ही है।”
– विवेकानंद
सनातन धर्म सुधार हेतु
“इस देश के तैंतीस करोड़ भूखे, दरिद्र और कुपोषण के शिकार लोगों को देवी – देवताओं के स्थान पर मन्दिरों में स्थापित कर वहां से देवी – देवताओं की मूर्तियों को हटा दिया जाये।” – विवेकानंद
पुरोहितवाद, ब्राह्मणवाद, धार्मिक कर्मकाण्ड और रूढ़ियों विरुद्ध आक्रमणकारी भाषा में इन विसंगतियों के विरुद्ध रहे। स्वामी जी के अनुसार सनातन धर्म सर्वश्रेष्ठ चिन्तकों के विचारों का निचोड़ है जो सम्पूर्ण संसार हेतु ईर्ष्या का विषय है। विदेशों की भौतिक समृद्धि को भारत की और भारत को भौतिक समृद्धि की जरूरत है। दोनों ही याचक के स्थान पर आपसी सामंजस्य स्थापित करना चाहिए।हमारे पास पश्चिम से अधिक बहुत कुछ है, जिसकी पश्चिम को आवश्यकता है।विवेकानंद के ओजस्वी और सारगर्भित व्याख्यानों की प्रसिद्धि संपूर्ण विश्व में है।
पुस्तकें एवं कृतियां –
1. संगीत कल्पतरु 1887 (वैष्णव चरण)
2. कर्म योग – 1896
3. राज योग – 1896, 1899 चोरीसवां एडिशन
4. Vedanta Philosophy – An address before the Graduate Philosophical Society (1896)
5. Lectures from Colombo to Almora (1897)
6. वर्तमान भारत (बांग्ला में उद्बोधन मार्च 1899)
7. My Master (1901) The Baker and Taylor Company, New York
8. Vedânta philosophy: lectures on Jnana Yoga (1902)
9. Vedânta Society, New York
10. ज्ञान योग (1899)
मरणोपरान्त प्रकाशित
11 .Addresses on Bhakti Yoga
भक्ति योग
12. The East and the West (1909)
13. Inspired Talks (1909)
14. Narada Bhakti Sutras अनुवाद
15. Complete Works – a collection of his writings, lectures and discourses in a set of nine volumes.
16.Seeing beyond the circle (2005)
मृत्यु –
जीवन के अन्तिम दिन 04 जुलाई 1902 को उन्होंने शुक्ल यजुर्वेद की व्याख्या करते हुए कहा
“एक और विवेकानन्द चाहिये, यह समझाने हेतु कि इस विवेकानन्द ने अब तक क्या किया है।”
इसके बाद ध्यान अवस्था में चले गए इसी ध्यानावस्था में ही ब्रह्मरन्ध्र को भेद कर महासमाधि ले ली। बेलूर में गंगा तट पर गुरु रामकृष्ण देव परमहंस के अंत्येष्टि स्थल के निकट चन्दन की चिता पर स्वामी जी की अंत्येष्टि की गई। उसी स्थान पर उनके अनुयायियों द्वारा अन्त्येष्टि स्थल पर ही एक मन्दिर बनवाया।
रामकृष्ण परमहंस मिशन –
रामकृष्ण मिशन ने विश्व में विवेकानन्द तथा रामकृष्ण परमहंस के सन्देशों के प्रचार हेतु 130 से अधिक केन्द्रों की स्थापना की।
“विवेकानंद के द्वितीय होने की कल्पना करना भी असम्भव है, वे जहाँ भी गये, सर्वप्रथम ही रहे। हर कोई उनमें अपने नेता का दिग्दर्शन करता था। वे ईश्वर के प्रतिनिधि थे और सब पर प्रभुत्व प्राप्त कर लेना ही उनकी विशिष्टता थी। हिमालय प्रदेश में एक बार एक अनजान यात्री उन्हें देख ठिठक कर रुक गया और आश्चर्यपूर्वक चिल्ला उठा-‘शिव!’ यह ऐसा हुआ मानो उस व्यक्ति के आराध्य देव ने अपना नाम उनके माथे पर लिख दिया हो।” – रोमां रोलां (एक लेखक)
“यदि आप भारत को जानना चाहते हैं तो विवेकानन्द को पढ़िये। उनमें आप सब कुछ सकारात्मक ही पायेंगे, नकारात्मक कुछ भी नहीं।”
– गुरुदेव रवीन्द्रनाथ ठाकुर
विशेष – स्वामी विवेकानंद नियमित रूप से शारीरिक व्यायाम एवं खेलों में भाग लिया करते थे। भारत में विवेकानंद के जन्म दिन को युवा दिवस के रूप में मनाया जाता है।
स्त्रोत
विभिन्न पत्रिकाएं एवं साइट्स पर स्वामी विवेकानंद के जीवन के बारे में लेख।
फोटो
गूगल के साभार
शमशेर भालू खां
जिगर चुरूवी

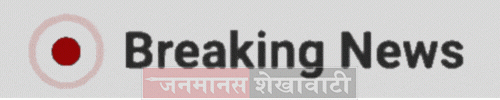

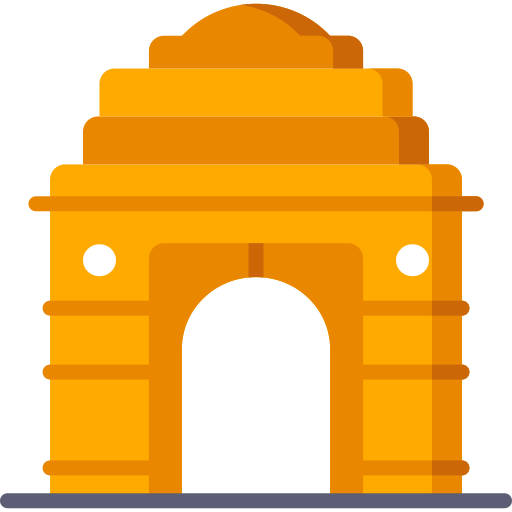 देश
देश विदेश
विदेश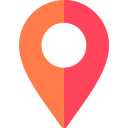 प्रदेश
प्रदेश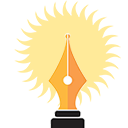 संपादकीय
संपादकीय वीडियो
वीडियो आर्टिकल
आर्टिकल व्यंजन
व्यंजन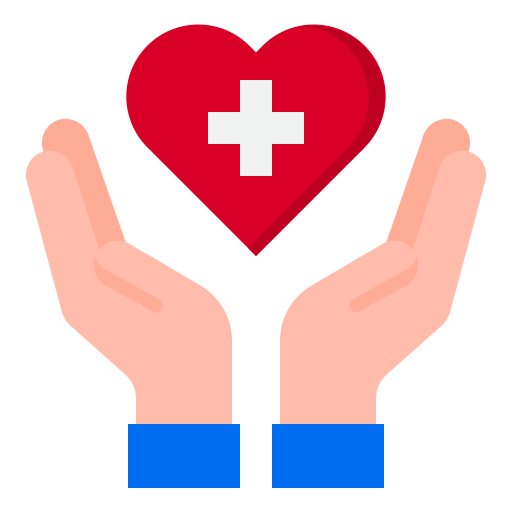 स्वास्थ्य
स्वास्थ्य बॉलीवुड
बॉलीवुड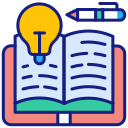 G.K
G.K खेल
खेल बिजनेस
बिजनेस गैजेट्स
गैजेट्स पर्यटन
पर्यटन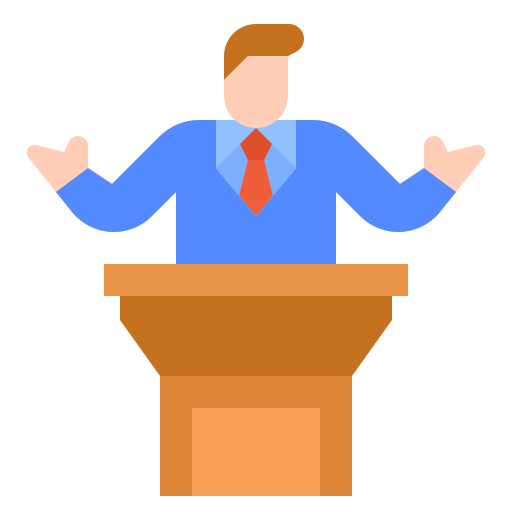 राजनीति
राजनीति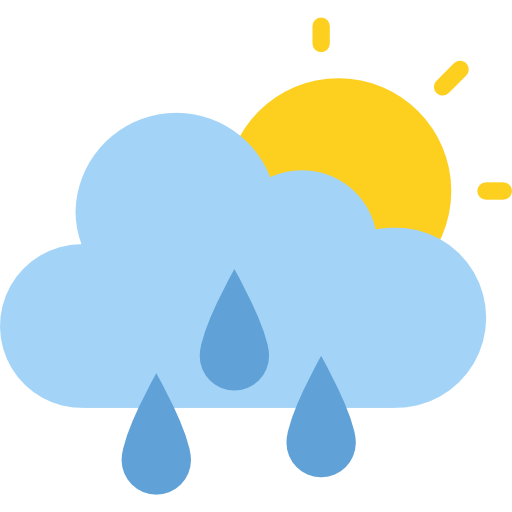 मौसम
मौसम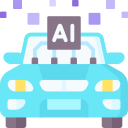 ऑटो-वर्ल्ड
ऑटो-वर्ल्ड करियर/शिक्षा
करियर/शिक्षा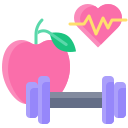 लाइफस्टाइल
लाइफस्टाइल धर्म/ज्योतिष
धर्म/ज्योतिष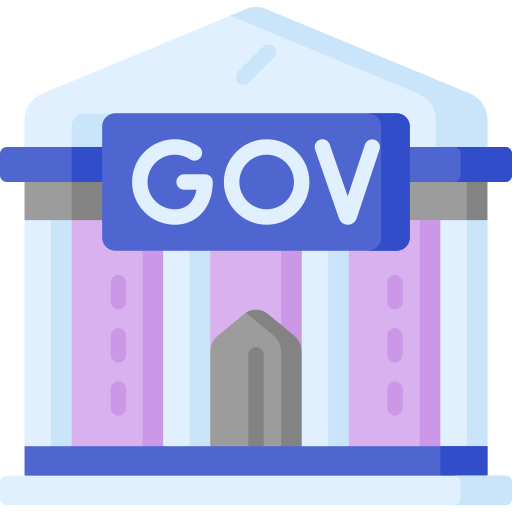 सरकारी योजना
सरकारी योजना फेक न्यूज एक्सपोज़
फेक न्यूज एक्सपोज़ मनोरंजन
मनोरंजन क्राइम
क्राइम चुनाव
चुनाव ट्रेंडिंग
ट्रेंडिंग Covid-19
Covid-19







 Total views : 1838838
Total views : 1838838



