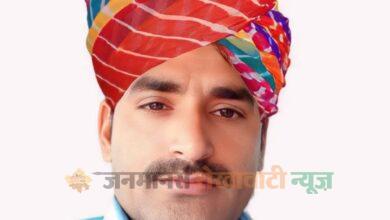21वीं सदी की आवश्यकता – भावनात्मक साक्षरता की अहमियत
स्कूलों में भावनाएं बोझ नहीं, बातचीत की शुरुआत बनती जा रही हैं


(प्रोग्राम लीडर, पीरामल फाउंडेशन, राजस्थान)
राष्ट्रीय शिक्षा नीति (एनईपी) 2020 ने भारतीय शिक्षा प्रणाली को केवल अंकों की दौड़ से बाहर निकालकर समग्र और मूल्य-आधारित शिक्षा की दिशा में एक नई दृष्टि दी है। यह नीति बताती है कि सच्ची शिक्षा वही है जो छात्रों के बौद्धिक विकास के साथ-साथ उनके सामाजिक, भावनात्मक और नैतिक पक्ष को भी मजबूत बनाए। इसी सोच के केंद्र में आता है – सामाजिक, भावनात्मक एवं नैतिक शिक्षण, जो केवल एक पाठ्यक्रम नहीं, बल्कि शिक्षा को मानवीय बनाने की एक व्यापक पहल है।
आज जब शिक्षा व्यवस्था में तेजी से बदलाव हो रहे हैं, यह और भी ज़रूरी हो गया है कि हम अपने बच्चों को सिर्फ किताबों के ज्ञान तक सीमित न रखें, बल्कि उन्हें जीवन के प्रति संवेदनशील और जिम्मेदार बनाएं।राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद (एनसीईआरटी)के 2022 सर्वेक्षणमें भी यह बात सामने आई कि43% विद्यार्थी स्कूलों में चिंता, उदासी या भावनात्मक तनाव महसूस करते हैं।ग्रामीण क्षेत्रों में प्रशिक्षित काउंसलर की अनुपस्थिति और भावनाओं को व्यक्त करने की सामाजिक कठिनाइयाँ इस स्थिति को और जटिल बनाती हैं, जिससे बच्चों की एकाग्रता, सीखने की इच्छा और आत्म-विश्वास पर सीधा असर पड़ता है।
इन्हीं चुनौतियों के समाधान के रूप मेंसामाजिक, भावनात्मक एवं नैतिक शिक्षणराजस्थान के अलग-अलग जिलों में; विशेष रूप सेझुंझुनूंमें एक बदलाव की लहर लेकर आया है। यह कार्यक्रमएमोरी यूनिवर्सिटी द्वारा विकसितऔर पीरामल फाउंडेशन के सहयोगसे लागू किया जा रहा है। इसका उद्देश्य है बच्चों और शिक्षकों दोनों में21वीं सदी की मुख्य क्षमताएँविकसित करना, जैसे – सहानुभूति, आत्म-नियंत्रण, जिम्मेदार निर्णय लेना, और सहयोगात्मक समस्या समाधान। ये सभी कौशल आज के जटिल, प्रतिस्पर्धी और लगातार बदलते सामाजिक परिदृश्य में आवश्यक हैं।
झुंझुनूंमें सामाजिक, भावनात्मक एवं नैतिक शिक्षणके क्रियान्वयन के दौरान हमने देखा कि कैसे छोटे-छोटे नवाचार – जैसे’इमोशन चेक’, ‘रेसिलिएंत जोन’, ‘ग्रेटीटीयुड बॉक्स’, ‘इमोशन ट्री’, और समुदाय आधारित पहल‘खुशियों का गुल्लक’ (जहाँ परिवार के सदस्य अपने सुखद पलों को साझा करते हैं) – बच्चों को न केवल अपनी भावनाओं को समझने और व्यक्त करने में मदद करते हैं, बल्कि उनके व्यवहार और संबंधों में भी सकारात्मक बदलाव लाते हैं।
शिक्षकों ने महसूस किया है कि कक्षा का तनाव घटा है और वे छात्रों से अधिक जुड़ाव महसूस कर रहे हैं। वहीं, ग्रामीण और कृषक पृष्ठभूमि से आने वाले माता-पिता अब अपने बच्चों की भावनात्मक ज़रूरतों को बेहतर ढंग से समझ रहे हैं और अधिक सक्रिय रूप से जुड़ रहे हैं। सी लर्निंग इनसाइट एप्प जैसे डिजिटल माध्यम इस ‘अदृश्य सीख’ को मापने और ट्रैक करने पर भी काम किया जा रहा है, जिससे शिक्षा और बाल विकास की पारंपरिक समझ को एक नई दिशा मिल रही है।
सामाजिक, भावनात्मक एवं नैतिक शिक्षण, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के उस सपने को धरातल पर उतार रहा है जहाँ शिक्षा का मकसद सिर्फ करियर नहीं, बल्कि चरित्र निर्माण, करुणा और जीवन के प्रति संवेदनशीलता है। मेरा व्यक्तिगत अनुभव यह बताता है कि झुंझुनूं से शुरू हुआ यह बदलाव आज पूरे राजस्थान की सरकारी स्कूल व्यवस्था में एक नई ऊर्जा भर रहा है – एक ऐसा बदलाव जहाँ किताबों और परीक्षाओं से आगे बढ़कर शिक्षा अब आत्म-जागरूक, संवेदनशील और जिम्मेदार नागरिकों के निर्माण की ओर अग्रसर है।
आज जब हम 21वीं सदी की चुनौतियों की बात करते हैं – जैसे मानसिक स्वास्थ्य, सामाजिक समरसता और वैश्विक नागरिकता – तब यह ज़रूरी हो जाता है कि हमभावनात्मक साक्षरता (Emotional Literacy) कोशैक्षणिक साक्षरता (Academic Literacy) जितना ही जरूरी मानें। तभी हम वास्तव में कह सकेंगे कि हम अपने बच्चों को भविष्य के लिए तैयार कर रहे हैं – न सिर्फ कामयाब बनने के लिए, बल्कि एक बेहतर इंसान बनने के लिए।
लेखक: मोहम्मद खुलूस ख़ान
(प्रोग्राम लीडर, पीरामल फाउंडेशन, राजस्थान)

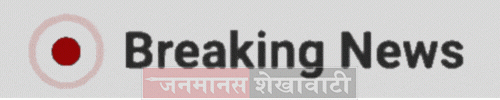

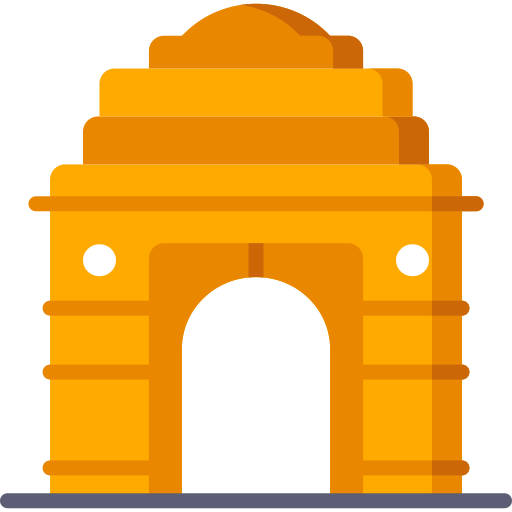 देश
देश विदेश
विदेश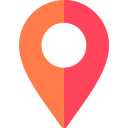 प्रदेश
प्रदेश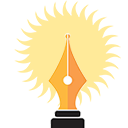 संपादकीय
संपादकीय वीडियो
वीडियो आर्टिकल
आर्टिकल व्यंजन
व्यंजन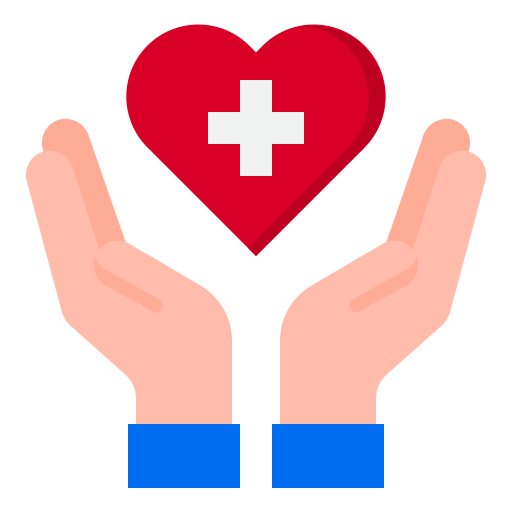 स्वास्थ्य
स्वास्थ्य बॉलीवुड
बॉलीवुड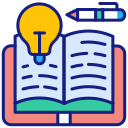 G.K
G.K खेल
खेल बिजनेस
बिजनेस गैजेट्स
गैजेट्स पर्यटन
पर्यटन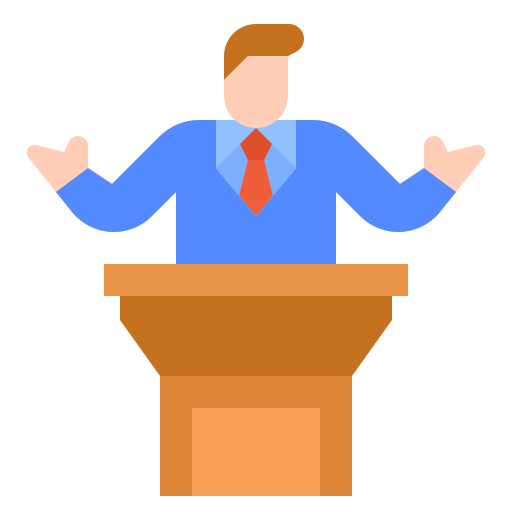 राजनीति
राजनीति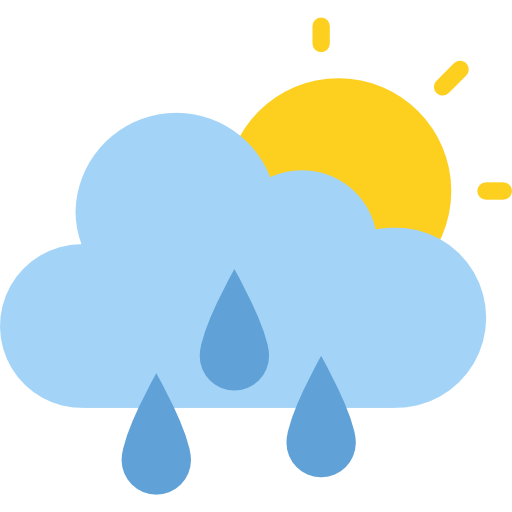 मौसम
मौसम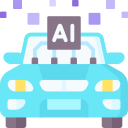 ऑटो-वर्ल्ड
ऑटो-वर्ल्ड करियर/शिक्षा
करियर/शिक्षा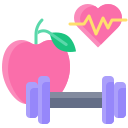 लाइफस्टाइल
लाइफस्टाइल धर्म/ज्योतिष
धर्म/ज्योतिष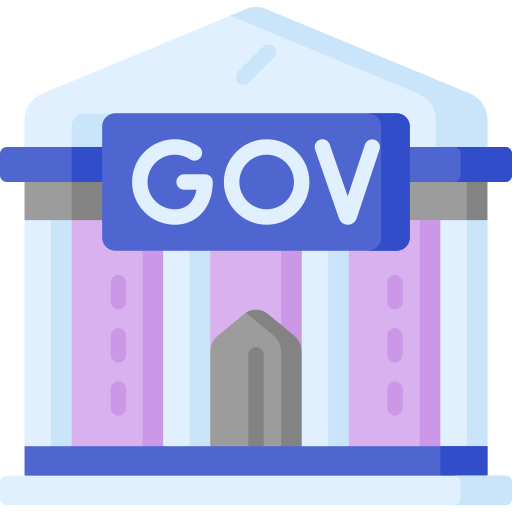 सरकारी योजना
सरकारी योजना फेक न्यूज एक्सपोज़
फेक न्यूज एक्सपोज़ मनोरंजन
मनोरंजन क्राइम
क्राइम चुनाव
चुनाव ट्रेंडिंग
ट्रेंडिंग Covid-19
Covid-19






 Total views : 2042196
Total views : 2042196